9 अगस्त का सूरज हर साल जब उगता है, तो यह केवल एक तारीख नहीं होती, यह एक पुकार होती है। यह दिन उन आवाज़ों का दिन है जिन्हें सदियों से दबाया गया, जिन्हें सभ्यता की भाषा में असभ्य कहा गया, जिन्हें विकास के नक्शे पर अदृश्य कर दिया गया। यह दिन आदिवासियों की जीवंत चेतना, उनकी संघर्ष-गाथाओं और उनके आत्मसम्मान के उद्घोष का दिन है। यह दिन केवल स्मरण का दिन नहीं है, यह विद्रोह की एक पुनरावृत्ति है जो बार-बार सत्ता के गलियारों को झकझोरता है। आदिवासी कोई परिभाषा नहीं, कोई आंकड़ा नहीं, कोई अनुसूची नहीं वे इस धरती की आत्मा हैं। वे उस सभ्यता के वारिस हैं जो न तो महलों में बसती है, न ही संसद की दीवारों में गूंजती है। वह जंगल की सांस में, पहाड़ों की नमी में, नदियों की लहरों में, और सबसे बढ़कर, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हर उस चेहरे में जीवित रहती है, जिसे भारत ने या तो विस्थापित किया या अनदेखा किया।जब संयुक्त राष्ट्र ने 1994 में इस दिन को अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में घोषित किया था, तब उसने यह स्वीकार किया था कि विश्व की मूलनिवासी सभ्यताएं विकास की दौड़ में सबसे अधिक कुचली गईं। भारत ने भी इसे अपनाया, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या भारत ने आदिवासियों को अपनाया है? क्या भारत ने बिरसा मुंडा, सिद्धो-कान्हू, रानी दुर्गावती की परंपरा को जीवित रखने का कोई सचेत प्रयास किया है, या फिर उनके नाम पर केवल स्मारक और घोषणाएं बनाईं?भारत के संविधान ने आदिवासी समाज को पहचान दी, पांचवीं और छठी अनुसूची में अधिकारों की बात की, लेकिन इतिहास ने उन्हें लगातार हाशिए पर धकेला। कभी वनवासी कह कर, कभी पिछड़ा कह कर, तो कभी विकास का बाधक कह कर। जब अंग्रेजों ने जंगलों पर कानून थोपे, तब आदिवासियों ने बगावत की। जब स्वतंत्र भारत ने खनन कंपनियों को जंगलों का पट्टा दिया, तब आदिवासी फिर लड़े। लेकिन हर बार उन्हें देशद्रोही कहा गया, नक्सली कह कर बंदूकें तानी गईं, सलवा जुडूम जैसे काले प्रयोग किए गए और ग्राम सभाओं को ताक पर रख दिया गया। लेकिन इस देश के पहाड़ों ने अब तक सब कुछ देखा है शोषण, प्रतिरोध और अब पुनरुत्थान। इस समय जब हम राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर बात कर रहे हैं, तब देश के कई हिस्सों में आदिवासी युवा अपनी बोली में शिक्षा की मांग कर रहे हैं, जल-जंगल-जमीन पर अपने स्वामित्व के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्परिभाषा कर रहे हैं। वे आरक्षण से आगे की राजनीति कर रहे हैं वे स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, वे यह नहीं मांग रहे कि उन्हें कोई अधिकार दिया जाए, वे कह रहे हैं कि उनका छीना गया अधिकार लौटाया जाए। आदिवासी समाज ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। उन्होंने कभी किसी के लिए दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। वे जंगल की संतान हैं उनकी रीढ़ में झुकना नहीं लिखा। वे जब विस्थापित होते हैं तो वे केवल घर नहीं खोते, वे अपने देवता खोते हैं, अपने पूर्वजों की हड्डियां, अपने त्योहार, अपनी मातृभाषा, अपने गीत और वह स्मृति जो पीढ़ियों से नृत्य करती आई थी। एक बाँसुरी जब टूटती है, तो वह केवल एक वाद्य नहीं टूटता। एक सभ्यता की धड़कन टूटती है। और भारत ने इन बाँसुरियों को न केवल तोड़ा, बल्कि उन पर चुप्पी का बोझ भी लाद दिया।आज देश की राजधानी में किसी नीति आयोग की रिपोर्ट जब कहती है कि आदिवासी सबसे अधिक ‘गरीब’ हैं, तो उसे यह भी कहना चाहिए कि आदिवासी सबसे अधिक ‘लूटे’ गए हैं। अगर गरीबी एक आंकड़ा है तो उसका दूसरा चेहरा है संपत्ति की लूट, संसाधनों की चोरी और सांस्कृतिक नरसंहार। किसने किया यह सब? केवल सरकारों ने नहीं, हम सबने। उस समाज ने जिसने जंगल को केवल लकड़ी समझा, जिसने नदी को केवल बिजली समझा, जिसने आदिवासी को केवल वोट समझा। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब आदिवासी समाज केवल प्रतिरोध नहीं कर रहा, वह पुनर्निर्माण कर रहा है। वह अपने गांवों में डिजिटल साक्षरता की बात कर रहा है, वह अपनी लोककथाओं को किताबों में बदल रहा है, वह विश्वविद्यालयों में अपनी भाषा को प्रवेश दिला रहा है, वह राष्ट्रीय धारा को चुनौती नहीं दे रहा, उसे अपनी धारा में ला रहा है। यह आत्मविश्वास भारतीय गणराज्य के लिए खतरा नहीं, शक्ति है। यह चेतना वह बुनियाद है जिस पर नया भारत खड़ा हो सकता है एक समावेशी, न्यायप्रिय, और प्रकृति-सम्मत भारत। सरकारें योजनाएं बनाएंगी, बजट देंगे, घोषणाएं करेंगी, लेकिन जब तक आदिवासी समाज निर्णयकर्ता नहीं बनेगा, तब तक ये सब अधूरे हैं। ग्राम सभाएं केवल प्रतीक नहीं होनी चाहिए, वे संविधान की जीवंत इकाई बनें। पेसा और वनाधिकार कानून को केवल क्रियान्वयन की फाइलों में नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। पुलिस और प्रशासन की भूमिका अब बदलनी चाहिए। वे हथियार नहीं, संवाद का माध्यम बनें।आदिवासी महिलाओं की भूमिका भी आज एक नई इबारत लिख रही है। वे अब जंगल से लकड़ी लाने वाली महिला नहीं रह गईं, वे जल-जंगल-जमीन की नेता बन रही हैं। वे अब दोहरी लड़ाई लड़ रही हैं पितृसत्ता और राज्यसत्ता दोनों से। और वे इस लड़ाई में न केवल जीत रही हैं, बल्कि नेतृत्व कर रही हैं।यह लेख कोई श्रद्धांजलि नहीं, एक एलान है। यह दिन केवल गीत-संगीत और सांस्कृतिक मेलों का उत्सव नहीं, बल्कि अपने हक की हुंकार का दिन है। जो समाज सदियों से अपने हिस्से का न्याय मांग रहा है, वह अब मांग से आगे बढ़कर स्वराज की भाषा बोल रहा है। आदिवासी अब भारत से नहीं, भारत को अपने साथ चलने को कह रहे हैं। यह राष्ट्र अगर सचमुच अपने संविधान को जीना चाहता है, तो उसे सबसे पहले आदिवासी समाज के साथ एक नया सामाजिक अनुबंध करना होगा। वह अनुबंध जिसमें कोई मुख्यधारा नहीं होगी और कोई हाशिया नहीं होगा। जिसमें सभी धाराएं एक साथ बहेंगी, समान गरिमा के साथ। भारत को अपनी आत्मा के आईने में देखना है तो उसे झारखंड, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुंदरगढ़, गोंदिया, मयूरभंज और दारांग के गांवों में जाकर देखना होगा। जहां बच्चे पेड़ों से बात करते हैं, जहां तालाबों में देवता बसते हैं, जहां नृत्य केवल उत्सव नहीं, प्रतिरोध है।जब अगली बार आप किसी पहाड़ पर चढ़ें, किसी जंगल से गुजरें, किसी नदी को पार करें — तो एक बार ठहरें और सोचें कि वहां कोई था, है और रहेगा। जो इस भूमि से केवल जीवन नहीं, आत्मा भी खींचता है। उस आत्मा का अपमान केवल अन्याय नहीं, आत्महत्या है। राष्ट्रीय आदिवासी दिवस हमें यह नहीं बताता कि हमें क्या करना है, यह हमें याद दिलाता है कि हमने क्या नहीं किया। यह एक शपथ लेने का दिन है कि अब आगे इतिहास नहीं दोहराया जाएगा, अब हम नई इबारत लिखेंगे। और वह इबारत तब तक अधूरी रहेगी जब तक इस देश की संसद में, इसके न्यायालयों में, इसकी नीतियों में, और सबसे ज़रूरी, इसके जन-मन में आदिवासी समाज बराबरी से नहीं बसेगा। इसलिए अब वक्त आ गया है कहने का जंगल बोलेंगे, पहाड़ गरजेंगे, और भारत बदलेगा।
Hazaribagh
 khabar365newsindiaAugust 8, 20251 Mins read71 Views
khabar365newsindiaAugust 8, 20251 Mins read71 Views
09 अगस्त- राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, जंगल बोलेंगे, पहाड़ गरजेंगे, भारत बदलेगा

Categories
Recent Posts
- कटकमदाग में पूर्व सदर विधानसभा प्रत्याशी मुन्ना सिंह ने कार्यकर्ताओं से किया संगठन मजबूत बनाने का आह्वान
- उप विकास आयुक्त ने किया कटकमसांडी प्रखंड का दौरा,मनरेगा,आवास एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक
- चौपारण घाटी लूटकांड का पुलिस ने किया महज दो घंटे में खुलासा — तीन अपराधी गिरफ्तार, लूटी गई पिकअप वैन, ब्रेज़्ज़ा, ₹21,300 नकद और मोबाइल फोन बरामद — हजारीबाग पुलिस की बड़ी सफलता
- पुलिस का ऑपरेशन क्लीन 22 चोरी की बाइक बरामद, 15 अपराधी दबोचे गए
- जेडीयू ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, 44 नामों पर लगी अंतिम मुहर
Related Articles
HazaribaghJharkhand  khabar365newsindiaOctober 14, 2025
khabar365newsindiaOctober 14, 2025
इंडियाज गोल्डन स्टार आइकॉन अवार्ड-2025 में वीरा पुस्तक के लेखक मनीष कुमार सम्मानित
Khabar365newsरांची। रांची के एक होटल में सोमवार को इंडियाज गोल्डन स्टार आइकॉन...
BreakingHazaribaghJharkhandझारखंडब्रेकिंगहजारीबाग  khabar365newsindiaOctober 13, 2025
khabar365newsindiaOctober 13, 2025
हजारीबाग जेल पर एसीबी का सख्त कदम, सुप्रीटेंडेंट से हुई लंबी पूछताछ
Khabar365newsहजारीबाग : जय प्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग के सुप्रीटेंडेंट जितेंद्र सिंह...
BreakingHazaribaghJharkhandझारखंडब्रेकिंगहजारीबाग  khabar365newsindiaOctober 13, 2025
khabar365newsindiaOctober 13, 2025
हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता, नक्सल विरोधी अभियान में काफी मात्रा में हथियार बरामद
Khabar365newsहजारीबाग : हजारीबाग पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) द्वारा चलाए...
Hazaribagh  khabar365newsindiaOctober 12, 2025
khabar365newsindiaOctober 12, 2025
कांग्रेसी कार्यकर्ता ” वोट चोर गद्दी छोड़ ” अभियान के लिए अपनी-अपनी कमर कस लें : जय प्रकाश भाई पटेल
Khabar365newsहजारीबाग : जिला कांग्रेस कार्यालय कृष्ण बल्लभ आश्रम में ” वोट चोर...


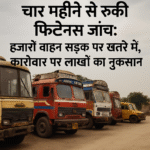





Leave a comment